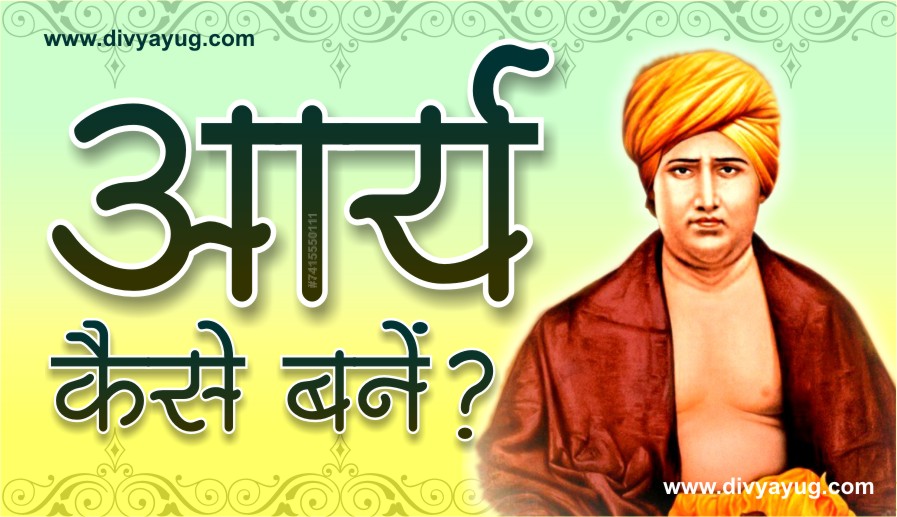ओ3म् इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्।
अपघ्नन्तो अराव्णः॥ ऋग्वेद 9।63।5॥
वेदमन्त्र कहता है कि परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए, सबको आर्य बनाते हुए, कृपण पापियों को परे हटाते हुए चले चलो।
वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का विशेष महत्त्व है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ । ईश्वर की सन्तान जो मनुष्य है वह शुभ और अशुभ दो गुणों की दृष्टि से दो भागों में बँटी हुई है- आर्य और अनार्य। आर्य वही हैं जिनका आचरण श्रेष्ठ है। ईश्वर को आर्य प्रिय हैं। महर्षि यास्क ने लिखा है- आर्यः ईश्वरपुत्रः। अर्थात् आर्य ईश्वर-पुत्र है। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है- अहं भूमिमददामार्याय। (ऋग्वेद 4.26.2) मैंने भूमि आर्य पुरुष के लिए प्रदान की है। गीता में भी आर्य शब्द की महत्ता प्रदर्शित की गई है-
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन॥ गीता 2.2॥
हे अर्जुन ! तुमको विषम-स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरूषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग देनेवाला है और न कीर्ति को करनेवाला है।
महर्षि दयानन्द जी सरस्वती ने हमें आर्य शब्द से पुनः परिचित कराया, अन्यथा हम इस शब्द को भूल चुके थे। आर्यत्व और मनुष्यता में नाममात्र का अन्तर है। आर्य और मनुष्य में भी नाममात्र का ही अन्तर है।
मन्त्र में चार बातें कही गई हैं- ईश्वर की स्तुति, श्रेष्ठ कर्मों का सम्पादन, विश्व को आर्य बनाना, अदानियों को हटाना। यदि ईश्वर की स्तुति, श्रेष्ठ कर्मों की सम्पन्नता और अदानशीलता के निवारण को साधन मान लिया जाए और आर्यत्व को साध्य तो इसमें कोई अनुचित बात न होगी। ईश्वर की स्तुति, श्रेष्ठ कर्मों का सम्पादन और अदानशीलता का निवारण- ये सब नैतिकता के अन्तर्गत आ जाते हैं। वस्तुतः सारी नैतिकता ही आर्यत्व के अन्तर्गत आ जाती है। आइए, हम विवेचन करें कि आर्यत्व के क्या साधन हैं? आर्यत्व के चार प्रमुख साधन हैं- सदाचार, कर्मकाण्ड, अर्थशुद्धि और सद्व्यवहार।
सदाचार- सदाचार की स्थिति आर्यत्व के साथ ऐसी ही है जैसे किसी पात्र में कोई खाद्य-पदार्थ रखने से पहले उस पात्र का मार्जन। किसी भी पात्र में कोई भक्ष्य वस्तु डालने से पहले उसका माँजना बहुत आवश्यक होता है। कर्मकाण्ड, अर्थशुद्धि और सद्व्यवहार को धारण करने से पहले आवश्यक है कि मनुष्य अपने व्यसनों का त्याग करें। जब तक व्यक्ति अपने व्यसनों का त्याग नहीं करता, तब तक उसके जीवन में निखार उत्पन्न नहीं हो सकता। सदाचार में सबसे पहले मादक द्रव्यों का निषेध आता है। मादक द्रव्यों के सेवन की बात आर्यत्व में इसलिए निषिद्ध है कि इन मादक द्रव्यों का मनुष्य की बुद्धि के साथ बहुत वैर है। जिसकी बुद्धि असन्तुलित हो गई, उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। वैदिक धर्म में बुद्धि के इन विनाशक तत्त्वों का विरोध किया गया है। मनु महाराज ने लिखा है- वर्जयेन्मधुमांसं च। (मनु स्मृति 2.177) मनुष्य शराब आदि मादक द्रव्यों से पृथक् रहे। मनु महाराज ने इसको राक्षसों और पिशाचों का पेय माना है। उर्दू के कवि के शब्दों में-
वो डूबे इस तरह कि फिर न उभरे जिन्दगानी में।
हजारों बह गये इन बोतलों के बन्द पानी में॥
बहता हुआ पानी तो मनुष्यो को बहाता ही है, परन्तु बोतलों का बन्द पानी भी हजारों व्यक्तियों को बहाकर ले जाता है। यह बोतलों का बन्द पानी शराब है। इसने लाखों मनुष्यों को बर्बाद करके रख दिया है-
उसकी बेटी ने उठा रक्खी है दुनिया सिर पर।
खैरियत गुजरी कि अंगूर के बेटा न हुआ॥
शराब को अंगूर की बेटी कहकर पुकारा गया है। अंगूर की सन्तान उसकी बेटी है। अंगूर के यहाँ अभी लड़का उत्पन्न नहीं हुआ। केवल लड़की ही उत्पन्न हुई है तब यह हाल है, यदि लड़का उत्पन्न होता तो न जाने क्या उत्पात होता?
शराब से व्यक्ति की शारीरिक हानि तो है ही, आर्थिक हानि भी होती है। बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक हानि तो है ही, सामाजिक अपयश भी होता है। इस व्यसन से हानि-ही-हानि है। शराबी को शरीर के रोग लग जाते हैं। इस व्यसन से धन की बहुत हानि हो जाती है। शराबी की मानसिक शक्ति शिथिल हो जाती है। बुद्धि विषय-विकारों की ओर दौड़ती है। इससे निश्चित ही आत्मा की हानि होती है। समाज में अपयश तो होता ही है। यही स्थिति अन्य व्यसनों की है।
वैदिक धर्म ने मांसाहार का विरोध इसलिए किया, क्योंकि इससे प्राणियों की हत्या होती है। वैदिक धर्म में सभी प्राणियों को ईश्वर की सन्तान स्वीकार किया गया है। एक सन्तान दूसरी सन्तान की हत्या अपनी उदरपूर्ति के लिए करे, यह कहाँ तब उचित है? वेद में तो पशुओं की शान्ति के लिए भी प्रार्थना की गई है-
इन्द्रो विश्वस्य राजति।
शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे॥ (यजुर्वेद 36.8)
अर्थात् परमैश्वर्यवान् परमात्मा सारे संसार पर शासन करता है। वह हमारे दो पैर वाले और चार पैर वालों के लिए कल्याणकारी हो।
यजमानस्य पशून् पाहि। (यजुर्वेद 1.1)
अर्थात् हे परमेश्वर ! तू यजमान के पशुओं की रक्षा कर। इस प्रकार वेद में यजमान के पशुओं की रक्षा का विधान किया गया है। मनु महाराज ने लिखा है-
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते॥ (मनुस्मृति 5.45)
जो जीव वध-योग्य नहीं हैं, उनको जो कोई अपने सुख के निमित्त मारता है, वह जीवित दशा में भी मृतक-तुल्य है। वह कहीं भी सुख नहीं पाता है।
यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति।
स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते॥ (मनुस्मृति 5.46)
जो मनुष्य किसी जीव को बन्धन में रखने, वध करने व क्लेश देने की इच्छा नहीं रखता है, वह सबका हितेच्छु है। अतएव वह अनन्त सुख भोगता है।
नोऽकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित्।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्॥ (मनुस्मृति 5.48)
जीवों की हिंसा बिना मांस की प्राप्ति नहीं होती और जीवों की हिंसा स्वर्ग-प्राप्ति में बाधक है। अतः मांस-भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए।
समुत्पत्तिं तु मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्।
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्॥ (मनुस्मृति 5.49)
मांस की उत्पत्ति, जीवों का बन्धन तथा उनकी हिंसा- इन बातों को देखकर सब प्रकार से मांस-भक्षण का त्याग करना चाहिए।
न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत्।
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते॥ (मनुस्मृति 5.50)
जो मनुष्य विधि त्यागकर पिशाच की तरह मांस-भक्षण नहीं करता वह संसार में सर्वप्रिय बन जाता है और विपत्ति के समय कष्ट नहीं पाता।
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चैति घातकाः॥ (मनुस्मृति 5.51)
पशु-हत्या की सम्मति देने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब घातक अर्थात् कसाई हैं।
फलमूलाशनैर्मेध्यैर्मुन्यन्नानां च भोजनैः।
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात्॥ (मनुस्मृति 5.54)
मनुष्य को सेब, केला आदि पवित्र फल, गाजर, मूली आदि कन्द-मूल और मुनी-अन्न (साँवा, तिन्नी आदि) के खाने से वह फल प्राप्त नहीं होता, जो मांस-भक्षण के परित्याग से प्राप्त होता है।
मांस भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्।
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ (मनुस्मृति 5.54)
विद्वज्जन मांस का यह लक्षण कहते हैं कि जिसके मांस को मैं इस जन्म में खाता हूँ, वह आगामी जन्म में मेरे मांस का भक्षण करेगा।
उपर्युक्त श्लोकों से यह ज्ञात होता है कि मनु महाराज मांस-भक्षण के कितने प्रबल विरोधी थे।
वैदिक धर्म ने तीसरा निषेध किया है ‘अश्लीलता‘ का। अश्लीलता का अर्थ है भद्दापन। भद्दे चित्र, भद्दे गाने, भद्दा साहित्य और स्त्रियों का नृत्य- इन चारों को अश्लीलता अर्थात् भद्देपन के अन्तर्गत लिया गया है। ये चारों वस्तुएँ कामुकता को बढावा देने वाली हैं, व्यक्ति में कामवासना को जाग्रत करने वाली हैं। व्यक्ति में जितनी कामुकता बढेगी, वह उतना ही स्त्रीसंग की इच्छा करेगा। जितना स्त्रीसंग करेगा, उतना ही परमेश्वर से दूर होगा। इन चारों वस्तुओं से बचने के लिए ही वेद ने कहा है-
भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्थिरैरंगैस्तुष्टवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ (यजुर्वेद 25.21)
हे विद्वान् जनो ! कानों से हम भद्र सुनते रहें। हे पूजनीय महात्माओ ! आँखों से हम शुभ देखते रहें। दृढ अंगों और शरीरों से स्तुति करते हुए हम लोग विद्वानों का जो हितकारी जीवन है उसे प्राप्त करें।
मन्त्र में विद्वानों के हितकारी जीवन की प्रार्थना की गई है। वह हितकारी जीवन दृढ अंगों से युक्त और ईश्वर की स्तुति करते हुए हो। यह कैसे प्राप्त हो? इसकी प्राप्ति के दो साधन बताए गये- कानों के द्वारा भद्रश्रवण और आँखों के द्वारा भद्रदर्शन।
ज्ञान-प्राप्ति के साधन हैं- आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा। इनमें प्रमुख है- आँख और कान। आँखों और कानों से हम बाहरी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया इस प्रकार है-
आत्ममनसोः संयोगविशेषात्संस्काराच्च स्मृतिः। (वैशेषिक 9.2.6)
जब आँख और कान (अथवा अन्य तीन ज्ञानेन्द्रियाँ) किसी पदार्थ के साथ सम्बद्ध होते हैं तो उस इन्द्रिय के साथ मन का संयोग होता है और मन के साथ आत्मा का। इस क्रमबद्ध प्रक्रिया से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से स्मृति का निर्माण होता है। स्मृति के पीछे संस्कार और संस्कारों के पीछे आत्मा और आत्मा के पीछे मन और मन के साथ इन्द्रिय-संयोग और इन्द्रिय के साथ पदार्थ का संयोग- यह एक क्रम है। इस क्रम में जो आदिम बात है वह है इन्द्रियों के साथ पदार्थों का संयोग। इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों में मुख्य इन्द्रियाँ हैं- आँख और कान। इन्हीं दोनों इन्द्रियों को पवित्र रखने के लिए कहा गया है कि आँखें अपवित्र दृश्यों को न देखें और कान अपवित्र शब्दों को न सुनें। जब कान और आँखें पवित्र हो जाती हैं तो संस्कार और विचार भी पवित्र होते हैं। जब आँखें और कान अपवित्र हो जाते हैं तब विचार और संस्कार भी अपवित्र हो जाते हैं और व्यक्ति नैतिक पतन की ओर अग्रसर होता है। नैतिक और आध्यात्मिक पतन के गर्त में गिरने से बचने का यही रास्ता है कि व्यक्ति कानों से पवित्र वचन सुने और आँखों से पवित्र दृश्य देखें। इसलिए अश्लील चित्र-दर्शन, अश्लील गीतश्रवण, अश्लील साहित्य का अध्ययन एवं नृत्य इत्यादि ये सब आँखों और कानों के बिगाड़ने के साधन बताये गये हैं।
चौथा निषेध है ‘दुराचार‘ का। दुराचार से अभिप्राय यहाँ परस्त्रीगमन से है। वैदिक धर्म ने ‘मातृवत् परदारेषु‘ की भावना को प्रतिष्ठित किया है। दूसरे की माता और भगिनी को हम अपनी माता और भगिनी समझें। परस्त्री-गमन को नैतिक पतन का एक बहुत बड़ा साधन माना गया है। हमारे पूर्वज इसी मर्यादा का पालन करते आये है। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र, योगेश्वर श्रीकृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी और भारत के अन्य सभी महापुरुष इसी पथ के पथिक रहे हैं। पूर्व और पश्चिम की सभ्यता में यही बहुत बड़ा अन्तर है। मनु महाराज ने लिखा है- स्वदारनिरतः सदा। (मनुस्मृति 3.45)
मनुष्य सदा अपनी पत्नी से ही सन्तुष्ट रहे। मनु जी का आशय यह है कि केवल अपनी पत्नी के साथ ही सन्तुष्ट रहे। परस्त्री का संग न करे। यह सदाचार आत्मिक पवित्रता का एक प्रमुख लक्षण माना गया है।
पाँचवाँ निषेध जुए का किया गया है। जुए का विरोध धर्म-शास्त्र ने इसलिए किया कि उसमें धन की प्राप्ति बिना परिश्रम के की जाती है। दूसरे की कमाई को मुफ्त में हड़पने की भावना मनुष्य में विद्यमान रहती है। वेद ने इसका निषेध किया है-
अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः।
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः॥ (ऋग्वेद 10.34.13)
ऋग्वेद के दसवें मण्डल के चौंतीसवें सूक्त के चौदह मन्त्रों में जुए के भयंकर परिणामों का कारूणिक चित्रण है। सूक्त के पहले मन्त्र में जुआरी की प्रसन्नता प्रकट की गई है। जुआरी जब मुफ्त का माल प्राप्त करता है तो कहता है कि जुए के पासे प्रसन्नता देते हैं और बहेड़े की लकड़ी का बना हुआ गोटा उसी प्रकार हर्षित करता है, जिस प्रकार मूंज के घिरे पर्वत में उत्पन्न सोम का रस हर्षित करता है।
जुए की हानियाँ गिनाते हुए वेद कहता है कि हारे जुआरी की सास भी उससे द्वेष करती है, पत्नी भी विरक्त हो जाती है, माँगने पर भी किसी धन देने वाले को वह नहीं पाता है। मूल्यवान् घोड़े के समान उसके सुख और रक्षा को कभी भी नहीं देखता हूँ। जुआरी की पत्नी को अन्य जुआरी हथियाकर तंग करते हैं। जुआरी के पिता, माता और भाई लोग कहते हैं कि वे उसको नहीं जानते हैं कि वह कौन है, बाँधकर इसे ले जाओ। वह ऋणग्रस्त होकर धन की इच्छा करता हुआ रात्रि में दूसरों के घर चोरी करने जाता है। जुआरी अपनी स्त्री और दूसरों की स्त्री, उनके उत्तम कर्म और गृह को देखकर मन में सन्तप्त होता है। वह दिन के पूर्वभाग में पासे जोड़ता है और रात्रि में सर्दी से बचने के लिए अग्नि के पास पड़ जाता है।
इस प्रकार उपर्युक्त शब्दों में वेद ने जुआरी की दुरवस्था का वर्णन किया है।
प्रश्न उठता है कि इन पाँचों व्यसनों का वेद ने निषेध क्यों किया है? ये पाँचों वस्तुएँ आत्मा की पवित्रता के रास्ते में अवरोधक हैं। परमात्मा शुद्धस्वरूप है। परमात्मा तक पहुँचने के लिए आत्मशुद्धि बहुत आवश्यक है। आत्मशुद्धि के लिए उपर्युक्त व्यसनों का त्याग अनिवार्य है।
आर्यत्व का दूसरा साधन है कर्मकाण्ड। वैदिक कर्मकाण्ड में कई बातें आती हैं। प्रातःकाल उठते समय और रात्रि में सोते समय महर्षि दयानन्द ने प्रत्येक आर्य के लिए क्रमशः पाँच और छह मन्त्रों के उच्चारण का विधान किया है। यह कर्मकाण्ड का पहला अंग है। प्रातःकालीन मन्त्रों में से पहला मन्त्र यह है-
प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरूणा प्रातरश्विना।
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोममुत रुद्रं हुवेम॥ (ऋग्वेद 7.14.1)
इन पाँच वेदमन्त्रों में परमात्मा के अनेक नाम गिनाये गये हैं। उसे अग्नि, इन्द्र, प्राणापान के समान प्रिय, सूर्य-चन्द्र का उत्पादक, सकल ऐश्वर्यमय, पुष्टिकर्त्ता, वेदज्ञान एवं ब्रह्माण्ड का पालक, जयशील, तेजस्वी, धारक, सबका जानने हारा, दुष्टों को दण्डदाता, सर्वप्रकाशक, भजनीय स्वरूप, सर्वोत्पादक, सत्याचार का प्रेरक, परमपूजित इत्यादि नामों और विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। फिर कुछ वस्तुएँ माँगी गई हैं। उससे प्रार्थना की गई है कि हमें प्रज्ञा दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। गाय और घोड़े आदि उत्तम पशुओं के योग से राज्यश्री को हमारे लिए प्रकट कीजिए। हम उत्तम मनुष्यों से बहुत वीर मनुष्यों वाले अच्छे प्रकार होवें। हम ऐश्वर्ययुक्त और शक्तिमान् होवें। हम लोग उत्तम प्रज्ञा और सुमति में सदा प्रवृत्त रहें। आप इस संसार और हमारे गृहाश्रम में अग्रगामी और सत्यकर्मों में वृद्धि करनेवाले हूजिए।
इस प्रकार परमात्मा को अपने जीवन का नेता मानकर उससे बहुत महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाएँ की गई हैं। महर्षि ने आर्यों में ईश्वर-विश्वास भरने के लिए यह विधि निश्चित की कि आर्य प्रातःकाल उठते ही ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थनाएँ करें। महर्षि ने यह भी विधान किया है कि सोते समय छह मन्त्रों का पाठ किया जाए। सोते समय मन पर विकार आक्रमण न कर सकें, इसके लिए ‘शिवसंकल्प‘ के मन्त्रों के पाठ का विधान किया गया है। पहला मन्त्र इस प्रकार है-
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति।
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ (यजुर्वेद 34.1)
रात्रि के समय मन पर काम-विकार आक्रमण न करें, इससे बचने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। मन के अनेक विशेषण गिनाये गये हैं। वह मन दूर-दूर तक जानेवाला, जागते हुए और सोते हुए का समान रूप से चलनेवाला, दूर-दूर ले जाने वाला, विषय-प्रकाशक इन्द्रियों का प्रकाशक, धर्मव्यवहार और विद्वानों के बीच कर्म करने का साधन, प्राणियों के भीतर अद्वितीय और पूजनीय, ज्ञान का उत्तम भण्डार, स्मरणशक्ति, धारणशक्ति, अमर ज्योति से मुक्त प्रत्येक कर्म का साधक, पूजनीय कर्म का फैलानेवाला, त्रयी विद्या का आधार, प्राणियों के विचार से ओतःप्रोत, इन्द्रियों का सारथि, सबका चालक, हृदय में स्थित और वेगवान् है। वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्पवाला हो जाए। इस प्रकार अठारह गुण गिनाकर छह बार मन को शिवसंकल्प वाला बनने की प्रार्थना की गई है।
वेद ने सन्धिवेला में सन्ध्या का विधान किया है। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों सन्धिवेलाओं में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। वेदमन्त्र कहता है-
उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्। नमो भरन्त एमसि॥ (ऋग्वेद 1.1.7)
हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! प्रतिदिन प्रातः एवं सायं अपनी बुद्धि से हम उपासक जन नमस्कार को धारण करते हुए आपके समीप प्राप्त होते हैं।
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपासीत, उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्। (षड्विंश ब्राह्मण प्रपाठक 4 खण्ड 5)
इसलिए दिन और रात के संयोग में अर्थात् सूर्य के उदय और अस्त होते समय सन्ध्योपासन करे। मनु महाराज ने लिखा है-
ब्राह्मे महूर्त्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्। कार्यक्लेशाँश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च॥ (मनुस्मृति 4.92)
ब्राह्ममहूर्त्त में उठे। धर्म, अर्थ, शरीर के रोग, उनके मूल का चिन्तन करे। वेतत्त्वार्थ अर्थात् ईश्वर का ध्यान करे।
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः।
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम्॥ (मनुस्मृति 4.93)
उठकर आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर, शौच-स्नान आदि करके प्रातः तथा सायं दोनों समय की सन्ध्या में चिरकालपर्यन्त जप करता रहे।
सन्ध्या का महत्त्व दर्शाते हुए कहा गया है-
न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्।
स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः॥ (मनुस्मृति 2.103)
जो प्रातःकालीन और सायंकालीन सन्ध्या नहीं करता, वह सब द्विजकर्मियों से शूद्र के समान बहिष्कार के योग्य है।
इसी प्रकार कहा गया है-
सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता।
स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः॥
जिसने सन्ध्या नहीं जानी और जिसने सन्ध्या का अनुष्ठान नहीं किया, वह सब द्विजकर्मियों से शूद्र के समान बहिष्कार करने के योग्य है।
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत् सावित्रीमार्कदर्शनात्।
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्॥ (मनुस्मृति 2.101)
प्रातःकाल की सन्ध्या और गायत्री का जप सूर्य के दर्शन होने तक करे और सायंकालीन सन्ध्या तबतक करे जबतक सितारे आकाश में भली-भाँति झलकने लगें।
ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वाद्दीर्घमायुरवाप्नुयुः।
प्रज्ञां यशश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च॥ (मनुस्मृति 4.94)
ऋषियों ने चिरकालपर्यन्त सन्ध्या करने से बुद्धि, विद्या, यश, कीर्ति तथा ब्रह्मतेज को प्राप्त किया है।
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम भी सन्ध्या किया करते थे, ऐसा रामायण से सुस्पष्ट है-
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते।
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्त्तव्यं दैवमाह्विकम्॥
तस्यर्षोः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ।
स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जपैतुः परमं जपम्॥
महर्षि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की विघ्न-निवृत्ति के लिए श्री रामचन्द्र व लक्ष्मण जी को लेकर चले तो रात्रि व्यतीत करने के लिए एक स्थान पर ठहरे। प्रातःकाल उन्होंने श्रीराम को पुकारा और कहा, ‘कौसल्या की सन्तान राम ! प्रातःकाल की सन्ध्या का समय हो गया है। तुम उठो और सन्ध्या-यज्ञ इत्यादि करो। उस ऋषि के परमोदार वचनों को सुनकर वे उठे और स्नान करके उन्होंने परम जप अर्थात् गायत्री का जाप किया।
माता सीता जी भी सन्ध्या करती थीं, ऐसा भी रामायण से पता चलता है-
हनुमान जी जब सीता जी को ढूँढते हुए अशोकवाटिका में पहुँचे तो सोचने लगे कि सीता जी यदि जीवित होंगी तो सन्ध्या करने के लिए अवश्य ही नदी के किनारे आएंगी-
सन्ध्याकालमनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी।
नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी॥
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना।
आगमिष्यति सावश्यमिमां शीतजलां नदीम्॥ (रामायण सुन्दरकाण्ड सर्ग 14.49,51)
श्री हनुमान जी सोच रहे हैं कि यह सन्ध्या का समय है, सन्ध्या में मन लगाने वाली और अक्षययौवना जनककुमारी सुन्दरी सीता सन्ध्याकालिक उपासना के लिए इस पुण्यसलिला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। यदि चन्द्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस शीतल जलवाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी।
इन उपर्युक्त उद्धरणों से सिद्ध होता है कि श्री रामचन्द्र व सीता जी दोनों सन्ध्योपासना करते थे।
इस प्रकार महाभारत के अनुसार योगेश्वर श्रीकृष्ण भी सन्ध्या उपासना किया करते थे-
अवतीर्य रथात् तूर्ण कृत्वा शौचं यथाविधि ।
रथमोचनमादिश्य सन्ध्यामुपविवेश ह ॥ (महाभारत उद्योगपर्व 84.21)
जब सूर्यास्त होने लगा तब श्रीकृष्ण शीघ्र ही रथ से उतरकर तथा घोड़ों को रथ से खोलने की आज्ञा देकर शौच-स्नान करके विधिपूर्वक सन्ध्योपासना करने लगे।
योगाभ्यास का अर्थ है मिलने का अभ्यास। प्रश्न है किसके मिलने का अभ्यास। इसका उत्तर है कि आत्मा-परमात्मा के मिलने का अभ्यास? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन के लिए अभ्यास किया जाता है। यम और नियम चरित्र-निर्माण के ही रूप हैं। आसन स्थिरतापूर्वक बैठने का नाम है। मन को स्थिर करने के लिए प्राणों का जो व्यायाम किया जाता है वह प्राणायाम कहलाता है। इन्द्रियों का उनके विषयों से निरोध करना प्रत्याहार है। चित्त का एक स्थान पर बाँधना धारणा कहलाता है। उस धारणा का बने रहना ध्यान कहलाता है। ध्यान की यही परिपक्वावस्था समाधि कहलाती है।
महर्षि दयानन्द ने परमेश्वर के ध्यान के फल के विषय में सत्यार्थ-प्रकाश के सातवें समुल्लास में लिखा है- ‘‘जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष-दुःख छूटकर परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा। परन्तु आत्मा का बल इतना बढेगा कि वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न माना कृतघ्नता और मूर्खता है।‘‘
कर्मकाण्ड का तीसरा अंग है यज्ञ। यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। यज्ञ का लक्ष्य जल और स्थल की शुद्धि है। यज्ञ इस शूद्धि का बहुत बड़ा साधन है। ‘‘जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इस पाप के निवारणार्थ उतना ही सुगन्ध को उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए।‘‘ महर्षि दयानन्द जी के इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ जल और स्थल की शुद्धि का साधन है। यज्ञ वेदमन्त्रों के साथ किया जाता है, अतः वह वेद के रक्षण का भी कारण बनता है। यह अन्तःकरण की शुद्धि का भी कारण होता है। इस प्रकार वैदिक कर्मकाण्ड में यज्ञ का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है।
वैदिक कर्मकाण्ड का चौथा अंग है वेद का स्वाध्याय। भारतीय वाङ्मय में वेदों का सर्वोच्च स्थान है। भारतीय ऋषियों ने वेद को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार किया है। इन्हें संस्कृति और सभ्यता का आधार माना है। इन्हें ज्ञान-विज्ञान का स्रोत स्वीकार किया है। इन्हें सत्यविद्याओं का आधार माना है। इनके पाठ को संसार के सभी ग्रन्थों के पाठ से ऊँचा स्वीकार किया है। इनके एक-एक शब्द को सार्थक स्वीकार किया है, एक-एक वाक्य को बुद्धिपूर्वक माना है। वेदों के सभी वचनों को सृष्टि-क्रमानुकूल स्वीकार किया है। इन्हें समस्त ज्ञान-विज्ञान का आधार स्वीकार करते हुए आध्यात्मिकता का परम पथ-प्रदर्शक स्वीकार किया गया है।
मनु ने लिखा है- वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। (मनुस्मृति 2.6) समस्त वेद को धर्म का मूल कहा गया है।
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते।
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ (मनुस्मृति 2.13)
जो अर्थ और काम में लिप्त नहीं हैं, उनके लिए ही धर्म का ज्ञान होता है। धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए वेद परम प्रमाण है।
जिस वेद की इतनी महिमा मनु जी ने गाई है, उस वेद के अध्ययन को परम धर्म स्वीकार करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा है-
संन्यसेत् सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्।
मनुष्य सब शुभकर्म भले ही छोड़ दे, परन्तु वेद का अध्ययन न छोड़े। इसीलिए महर्षि दयानन्द जी ने लिखा है- ‘‘वेद का पढना-पढाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है।‘‘
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः।
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्॥ (मनुस्मृति 2.6)
श्रुति (वेद) और स्मृति (शास्त्र) के द्वारा उदित धर्म का पालन करने से ही मनुष्य इस संसार में कीर्ति प्राप्त करता है और मरकर उत्तम सुख प्राप्त करता है। यहाँ वेदानुकूल आचरण को सुख का कारण बताया गया है।
सर्व तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा।
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै॥ (मनुस्मृति 2.8)
मनुष्य सम्पूर्ण वेद, शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और अपनी आत्मा के अविरुद्ध इन सबसे अच्छे प्रकार विचारकर, ज्ञाननेत्र से देखकर, श्रुतिप्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। ऐसा कहकर वेदानुकूल आचरण पर बल दिया गया है।
स्वाध्याय के दो अर्थ हैं- सत्पुरुषों के बनाये हुए ग्रन्थों का अध्ययन और अपने व्यक्तित्व का अध्ययन, जिसके द्वारा अपने दोषों को दूर करना और अपने को गुणों से भरपूर करना। यहाँ स्वाध्याय से यही अभिप्राय है। योगदर्शन में महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है-
शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। (योगदर्शन 2.32)
योगदर्शन में यम और नियमों का वर्णन किया गया है। इनमें एक नियम है स्वाध्याय का। सद्ग्रन्थों का अध्ययन योग-पथ पर चलनेवाले के लिए परमावश्यक है। प्राचीनकाल में स्नातक बनते समय आचार्य स्नातकों को यह उपदेश दिया करते थे-
स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम्। (तैत्तिरीयोपनिषद् 2.1) स्वाध्याय करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए।
किस प्रकार के ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए, मनु महाराज ने इस बात की ओर संकेत किया है-
बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च।
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाँश्चैव वैदिकान्॥ (मनुस्मृति 4.19)
बुद्धि की वृद्धि करने वाले, धन की वृद्धि करने वाले और हितकारी वेदोक्त ग्रन्थों एवं शास्त्रों का अध्ययन करता रहे।
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति।
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते॥ (मनुस्मृति 4.20)
जैसे-जैसे पुरुष शास्त्रों को यथावत् जानता है, वैसे-वैसे ही उस विद्या का विज्ञान बढता जाता है और उसी में रुचि भी बढती रहती है।
हमें किन-किन ग्रन्थों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, मनु महाराज ने इसका भी निर्देश किया है-
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः।
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः॥ (मनुस्मृति 12.95)
संसार को दुःखसागर में डुबोने वाले जो ग्रन्थ वेदबाह्य (वेद विरुद्ध) कुत्सित पुरुषों के बनाये हैं, वे सब निष्फल, असत्य, अन्धकार रूप इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं।
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्।
तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥ (मनुस्मृति 12.96)
जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं, वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उनका मानना निष्फल और झूठा है।
‘अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः‘ कहकर मनु ने स्वाध्याय को ब्रह्मयज्ञ के अन्तर्गत रखा है। स्वाध्यायेनार्चयेदृषीन्‘ कहकर मनु ने इसे ऋषियों की उपासना बताया है।
इस प्रकार वेदोक्त, ऋषिकृत ग्रन्थों और आत्मोन्नति के साधक ग्रन्थों का नाम ही स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय की पवित्रता और उच्चता बनाये रखने के लिए स्वाध्याय से पूर्व भी कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। उन प्रतिबन्धों का पालन करते हुए स्वाध्याय करना है। तभी स्वाध्याय फलीभूत होता है, अन्यथा नहीं। इस प्रतिबन्ध से एक बात और सिद्ध होती है कि स्वाध्याय के साथ आचरण की पवित्रता भी बहुत आवश्यक है। तैत्तिरीयोपनिषद् के ऋषि ने अध्ययन के साथ-साथ इन बातों के आचरण को भी आवश्यक बताया है।
यथार्थ आचरण, धर्मानुष्ठान करते हुए, बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोकते हुए, मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटाते हुए, मनुष्य-सम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए, ऊर्जा की रक्षा और वृद्धि करते हुए स्वाध्याय और प्रवचन करें।
महात्मा गान्धी के शब्दों में ‘‘कोई-न-कोई अच्छी पुस्तक पढते रहने से बुद्धि की वृद्धि होती है।‘‘ श्री बालगंगाधर तिलक के शब्दों में ‘‘मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा। क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ ये होंगी, वहाँ आप ही स्वर्ग बन जाएगा।‘‘
वस्तुतः सद्ग्रन्थ अच्छे मित्र के समान होते हैं। वे सन्मार्गदर्शक होते हैं। वे सद्विचार, सत्प्रेरणा और सत्कर्म के प्रेरक होते हैं। वे अन्धकार में प्रकाश का काम करते हैं। वे एकान्त में अच्छे साथी होते हैं। वे माता-पिता के समान अपने पाठक के हितचिन्तक होते हैं। वे सद्गुरु के समान अज्ञान के नाशक होते हैं।
कर्मकाण्ड का छठा अंग है ‘सत्संग‘। सत्संग की बहुत महिमा है। वास्तव में सन्ध्योपासना, स्वाध्याय और सत्संग- ये तीनों ही सत्संग हैं। सन्ध्योपासना ईश्वर का संग है। स्वाध्याय उन व्यक्तियों का परोक्ष संग है जो हमारे सम्मुख उपस्थित तो नहीं, परन्तु हम उनके वचनों का पाठ करते हुए उनका परोक्ष-संग करते हैं। सत्संग तो सज्जन पुरुषों का संग है ही। जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए सत्संग परमावश्यक है। स्वाध्याय से पहला पग जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, वह है सत्संग। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए भर्तृहरि जी ने बहुत ही सुन्दर कहा है-
जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मनोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति।
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्॥ (भर्तृहरि नीति शतक)
सत्संग बुद्धि की जड़ता का हरण करता है, वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा करता है, सम्मान को बढाता है, पाप का नाश करता है, मन को प्रसन्नता देता है, दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करता है। बताओ, सत्संगति मनुष्य का क्या-कुछ (कल्याण) नहीं करती है! किसी ने क्या सुन्दर कहा है-
धर्मं प्रसंगादपि नाचरन्त्यधर्मं प्रयत्नेन समाचरन्ति।
आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोकेऽमृतं परित्यज्य विषं पिबन्ति॥
मनुष्य प्रसंगवश भी धर्म का आचरण नहीं करते, परन्तु अधर्म का आचरण यत्नपूर्व करते हैं। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि लोग अमृत को छोड़कर विष का पान करते हैं।
सत्संग मूर्खों को विद्वान बनाता है, दुराचारियों को सदाचारी बनाता है, अप्रसिद्ध व्यक्तियों को यश देता है।
आर्यत्व का तीसरा आधार है- अर्थशुद्धि। अर्थशुद्धि से अभिप्राय यह है कि आजीविका के साधन पवित्र होने चाहिएँ। श्रमिक की आर्थिक पवित्रता इसमें है कि वह परिश्रमपूर्वक कार्य करे। श्रम-काल में समय नष्ट न करे। लिपिक, कर्मचारी, अध्यापक, प्राध्यापक और अधिकारी की आर्थिक पवित्रता इसमें है कि सरकारी माल की चोरी न करें, घूस न लें, अपने कार्यसमय में सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करें। व्यापारी की आर्थिक पवित्रता इसमें है कि वह मिलावट, धोखेबाजी, तस्करी और कालाधन कमाने से बचे। धन की यह पवित्रता श्रेष्ठ सन्तान का निर्माण करती है।
आर्यत्व का चौथा आधार है- सद्व्यवहार। सद्व्यवहार से अभिप्राय है अच्छा व्यवहार। हमारा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सद्व्यवहार और सदाचार तीन प्रकार का होता है- मानसिक, वाचिक और शारीरिक। मन का चिन्तन मानसिक व्यवहार, वाणी के वचन वाचिक व्यवहार और शरीर के कर्म शारीरिक व्यवहार कहलाते हैं। मनु महाराज ने लिखा है-
मानसं मनसैवायमुपभुंक्ते शुभाऽशुभम्।
वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनैव च कायिकम्॥ (मनुस्मृति 12.8)
मनुष्य मन के द्वारा किये गये पाप का फल मन से, वाणी के द्वारा किये गये कर्म का फल वाणी से और शरीर के द्वारा किये गये कर्म का फल शरीर से प्राप्त करता है। व्यवहार मनुष्य का दर्पण होता है। जिसमें मनुष्य के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। मनुष्य का पहला प्रभाव शरीर का, दूसरा उसकी वेषभूषा का, तीसरा उसकी वाणी का और चौथा उसके व्यवहार का होता है। व्यवहार का प्रभाव ही वास्तविक प्रभाव होता है। शारीरिक व्यवहार में सेवा करना, चोरी न करना, अहिंसा, दान, व्यभिचार-त्याग और इन्द्रियों को दुष्कर्मों से परे रखना आदि कर्म आते हैं। वाणी के व्यवहार में थोड़ा बोलना, सोच-समझकर बोलना, प्रेमपूर्वक बोलना, पीठ-पीछे किसी की निन्दा, आलोचना और उपहास न करना, सामने किसी का दिल दुखाने की बातें न करना, वचन-पूर्ति का ध्यान रखना, अश्लील बातें न करना, गालियाँ न देना, झूठ न बोलना, लड़ने-झगड़नेवाली बातें एक-दूसरे से न करना, आगे कुछ और पीछे कुछ कहने से बचना, अपनी प्रशंसा स्वयं न करना और गर्वोक्तियाँ न करना- ये सब बातें वाचित व्यवहार में आती हैं। मानसिक व्यवहार में मन के भावों की प्रधानता आती है। जैसे मन के भाव होंगे, वैसा ही वाणी और शरीर का आचरण होगा। जैसे मन के भाव होंगे, वैसा ही वाचिक और शारीरिक व्यापार होगा। वाचित और शारीरिक व्यवहार की उत्कृष्टता के लिए मानसिक भावों का उत्कृष्ट होना परमावश्यक है।
सदाचार, अर्थशुद्धि, कर्मकाण्ड और सद्व्यवहार के समन्वय का ही नाम आर्यत्व है। आर्यत्व एक साधना है। जो व्यक्ति इस साधना को करता रहेगा, वही वास्तव में आर्य रहेगा। आर्यत्व तो प्रतिदिन निरीक्षण की वस्तु है। जो प्रतिदिन निरीक्षण करता रहेगा, वही आर्य बन पाएगा। आर्यत्व केवल एक ही दिन धारण करने की वस्तु नहीं, अपितु यह तो प्रतिदिन धारण करने की वस्तु है। साभार वेद सन्देश - प्रो. रामविचार
How do we become Arya? | Vedic literature | Special importance of the word Arya | Meaning of the word Arya | Importance of the word Arya in the Gita too | Praise to The Lord | Virtue | Ritual | Meaningfulness | Good Behavior | Children of God | Virtuous Spiritual Purity | Divine Pure Form | Aryatva A Sadhana | Vedic Motivational Speech & Vedas Explained (Introduction to the Vedas, Explanation of Vedas & Vaidik Mantras in Hindi) for Maudaha - Kambam - Ajnala | दिव्ययुग | दिव्य युग |